

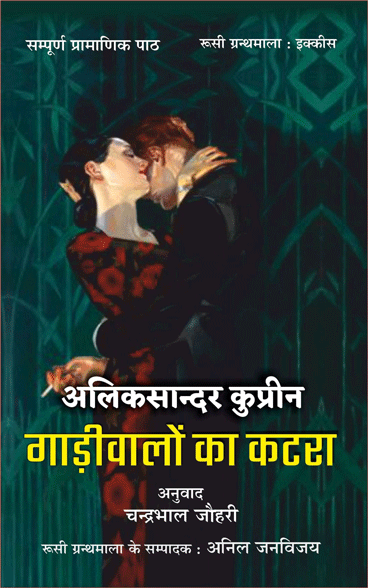


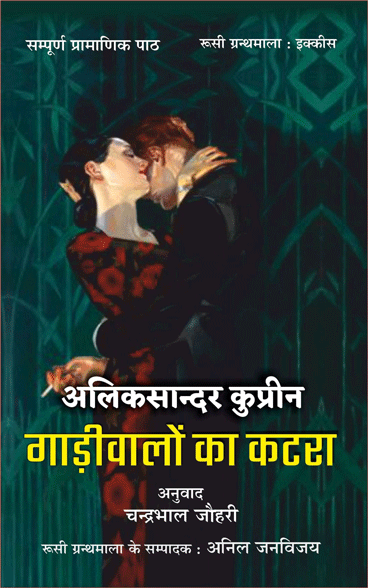

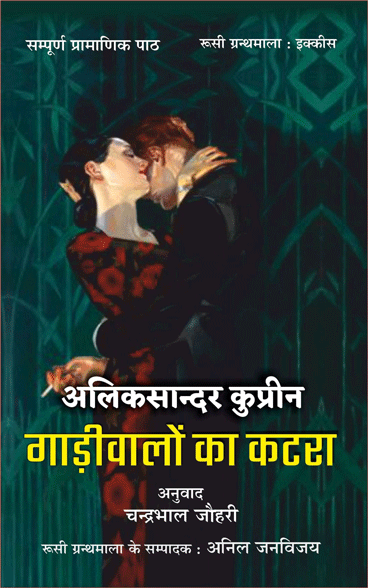


GARIWALON KA KATRA / गाड़ीवालों का कटरा
₹499.00 Original price was: ₹499.00.₹450.00Current price is: ₹450.00.
FREE SHIPMENT FOR ORDER ABOVE Rs.149/- FREE BY REGD. BOOK POST
Read eBook in Mobile APP
अलिकसान्दर कुप्रीन की प्रस्तावना
सचमुच मानव-समाज के सामने बहुत-सी ऐसी कठिन, भयंकर और असाध्य दीखनेवाली समस्याएँ हज़ारों वर्षों से हैं, जिनके बोझ से उसकी कमर टूटी जा रही है और जिनके कारण कभी-कभी तो वह पशु-समाज की तरह नीच दीखने लगता है। युद्ध, वेश्यावृत्ति, फाँसी, अधपेट मज़दूरी के लिए तनतोड़ मेहनत, थोड़े-से खाते-पीते लोगों का बहुसंख्य भुखमरे लोगों पर अधिकार इत्यादि मनुष्य-समाज की ऐसी ही भयंकर समस्याएँ हैं।
परन्तु इन सबमें स्त्री के शरीर का व्यापार, स्त्री के उस प्रेम का व्यापार जो कि मनुष्य जाति को ईश्वर की उच्चतम देन है, मुझे सबसे बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मनुष्य-समाज की इस पुरानी बीमारी का इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। मैं सोचता हूँ, मनुष्य से यह कहने की ज़रूरत है कि ‘देखो भाई, तुम्हारे घर में भी एक सफ़ेद बालोंवाली बूढ़ी दादी है जिससे तुमने बचपन में पहले-पहल लोरियाँ और कहानियाँ सुनी थीं, और जो अब तुम्हारे घर की छत और अभिमान हैं। तुम्हारे घर में भी एक माँ है जिसके स्तनों का मीठा-मीठा दूध तुम लोभ और आनन्द से–अपना सिर उसकी छाती में घुसेड़कर– पिया करते थे। तुम्हारे घर में भी एक पत्नी है जो तुम्हारे बच्चों की जननी और तुम्हारे कुल की गृहिणी है। तुम्हारे घर में भी एक छोटी-सी बहन है जिसका मधुर स्वर कोयल के संगीत की तरह तुम्हारे कानों में गूँजता है। इस बात के विचारमात्र से ही कि कोई तुम्हारी प्यारी बहन के सामने अश्लील शब्द मुँह से निकाले या हावभाव करे, तुम्हारी आँखों में खून उतर आता है और तुम्हारे जबड़े काँप उठते हैं; और ऐसी हरकत कोई आपकी लाड़ली बेटी के सामने करने की हिम्मत करे, तो फिर कहना ही क्या!
‘परन्तु फिर भी आप बाज़ार में बैठनेवाली स्त्रियों के पास अपना पैसा ठनकाते हुए उनका प्रेम खरीदने के लिए जाने की हिम्मत करते हैं– उस प्रेम को खरीदने के लिए जिसका परिणाम और एकमात्र उद्देश्य नवजीवन का संचार है, जो कि भगवान की सबसे रहस्यपूर्ण लीला है।
‘आप कहेंगे कि आप तो बाज़ार में बैठनेवाली ऐसी स्त्रियों के पास जाते हैं जो पतित हैं। परन्तु आपने कभी यह भी सोचने का कष्ट किया है कि वे क्यों पतित हैं? क्या यह सच नहीं है कि जिन स्त्रियों को आप पतित कहते हैं उन्हें यदि बचपन और जवानी में अच्छा लालन-पालन, स्नेहपूर्ण वर्ताव और उचित शिक्षा मिली होती तो वे भी आज आपके घर में बैठनेवाली माँ, आपकी स्नेहमयी बहन और आपकी लाड़ली पुत्री की ही तरह ऊँची और पवित्र होतीं?
‘अथवा आप यह सोचते होंगे कि मेरा घर और बात है और दूसरे का घर और बात। दूसरे के घर से आपको क्या मतलब? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्या आपने कभी यह भी सोचने का कष्ट किया है कि आपमें और हिंसक पशु में ऐसी अवस्था में क्या फर्क रह जाता है? आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप एक समाज में रहते हैं जिसका क़ायम रहना आपके हिंसक विचारों के चलते असम्भव है! और आप यह कैसे भूलते हैं कि आप अपने आपको शिक्षित, शिष्ट और धार्मिक भी कहते हैं?
‘यह भी याद रखिए कि जिस समय आप अपनी पशुवृत्ति को पूरा करके वेश्या के घर से चलने लगते हैं उस समय आपके मन में आत्मग्लानि होती है और आप उस वेश्या से, जिसे आप अधम समझते हैं, कहीं ज़्यादा अधम होते हैं, क्योंकि आप जीवन में गरीबी और अमीरी के अभागे फर्क का फ़ायदा उठाकर एक स्त्री का सर्वस्व उसी तरह लूटते हैं, जिस तरह कोई अन्धे को लूटता है, अथवा किसी अपाहिज के मुँह पर थप्पड़ मारता है अथवा किसी बालक को छलता है…’
मैंने जो कुछ मैं जानता था और जो कुछ मैं लिख सकता था, वेश्यावृत्ति के विरुद्ध लिखा है। परन्तु मुझे इस रोग के विरुद्ध कोई ऐसा अचूक नुस्खा नहीं मिला है जो मैं आपको बता दूँ। मैं तो सिर्फ़ इतना ही जानता हूँ कि वेश्यावृत्ति स्त्रियाँ खुशी से नहीं करतीं, मजबूरी से करती हैं। गरीबी, अज्ञान और लालच के कारण अथवा रोटी कमाने का और कोई जरिया न होने से ही स्त्रियों को यह अधम पेशा करना पड़ता है, अस्तु इन कारणों का ज़िक्र करना और इस अधम व्यवसाय और जीवन का हाल लिखना मैंने व्यर्थ नहीं समझा। मैं समझता हूँ कि सच्ची बातों और सच्चे दृश्यों का, चाहे वह कितने ही भयंकर क्यों न हों, मनुष्य पर सच्चा ही असर होता है।’
एक बार मैं सैण्टपीटर्सबर्ग से क्रीमिया जा रहा था। रास्ते में, रेलगाड़ी में कुछ नौजवान इंजीनियरों ने मुझे पहचान लिया और मुझसे कुछ वार्तालाप करने की इजाजत चाही। बातचीत में वे कहने लगे–
‘देखिए, आप वेश्यावृत्ति का विरोध तो करते हैं, परन्तु जवानी में जो कामदेव आदमी को मतवाला करता है, तब उसकी तृप्ति के लिए आप कौन-सा मार्ग दिखाते हैं?’
मैं जो मार्ग जानता था, उन्हें दिखाने लगा–
‘चौकी या कठोर चारपाई पर सोइए। खुरदुरी चादर बिछाइए, गुदगुदी या चिकनी नहीं। इतने कपड़े न ओढ़िए कि शरीर अधिक गरम हो जाय। सोने का कमरा खुला, हवादार और ठण्डा होना चाहिए। नींद गहरी लेनी चाहिए, परन्तु अधिक देर तक नहीं। सुबह को जल्द उठना चाहिए, ठण्डे पानी से स्नान करना चाहिए। खाना सादा और कम मसाले का हो। हो सके तो बिना मसाले का खाना चाहिए। अच्छा ओजस्वी और वीरतापूर्ण साहित्य पढ़ना चाहिए। खूब परिश्रम करना चाहिए और खुली हवा में खेलना चाहिए। लड़के और लड़कियों की सहपाठशालाएँ होनी चाहिए, जिनमें वे साथ-साथ पढ़ें। पच्चीस वर्ष की उम्र के लगभग विवाह हो जाना चाहिए।’
नौजवानों ने उत्तर में मुझसे कहा– ‘यह सब तो हम भी जानते हैं, परन्तु इन उपायों से मुख्य समस्या तो हल नहीं होती। कामवासना की तृप्ति के लिए आप कौन-सा मार्ग बताते हैं?’
इस पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने भी उन्हें वही कठोर उत्तर दिया जो कि एक बार तोलस्तोय ने दिया था।
एक बार पढ़े-लिखे रूसी आदमियों की एक बड़ी सभा में तोलस्तोय अपने समय की रूसी सरकार की कड़ी आलोचना कर रहा था। एक नौजवान ने उठकर उनसे प्रश्न किया– ‘अच्छा तोलस्तोय, मान लो कि जैसा तुम कहते हो, यह सरकार बिलकुल वैसी ही निकम्मी है और नष्ट कर डालने के योग्य है, परन्तु इसे नष्ट करने के बाद इसके बदले तुम हमें क्या दोगे?’
तोलस्तोय ने जलकर कहा– ‘मान लो कि आपको, भगवान न करे ऐसा हो, आतशक हो जाती है। आप आकर मुझसे कहते हैं कि मुझे यह बुरी बीमारी हो गयी है और मैं आपसे फौरन डाक्टर से जाकर इलाज कराने को कहता हूँ। इस पर आप मुझसे पूछते हैं– पर यह तो बताइए कि डाक्टर के यहाँ जाकर मैं इस बीमारी से तो मुक्त हो जाऊँगा, परन्तु आतशक के बदले फिर आप मुझे क्या देंगे?… मैं मानता हूँ भाई साहब, आपके ऐसे प्रश्न का उत्तर देना मुझे कठिन हो जायेगा…’
…इसी पुस्तक से…
- Description
- Additional information
Description
Description
इस नए संस्करण की भूमिका
‘गाड़ी वालों का कटरा’ नाम से हिन्दी में अनूदित अलिकसान्दर कुप्रीन के इस उपन्यास का मूल रूसी नाम है — ‘यामा’ यानी गड्ढा। यह रूसी नाम भी कुप्रीन ने इस उपन्यास को इस आधार पर दिया था कि जिन चकलों का इस उपन्यास में ज़िक्र किया गया है, वे उस बस्ती में बसे हुए हैं, जिसे पहले तांगेवालों की बस्ती यानी ‘यिमस्काया स्लाबदा’ के नाम से जाना जाता था। रेल, ट्राम, बस और कारें आने की वजह से तांगेवालों का धन्धा धीरे-धीरे ख़त्म हो गया। तांगेवालों की बस्ती उजड़ गई और किसी ने उस कटरे (बस्ती) में मज़दूरों, कारीगरों और सिपाहियों के लिए एक सस्ता-सा कोठा खोल दिया। बाद में धीरे-धीरे जब कोठे में भीड़ बढ़ने लगी, तो उस सस्ते कोठे के सामने ही एक थोड़ा उससे बेहतर क़िस्म का एक और चकला खुल गया। इस चकले में थोड़ा बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध थीं और उसमें आने वाले लोग भी मध्यवर्ग के यानी वक़ील, क्लर्क, छोटे-मोटे सरकारी अधिकारी और अफ़सर, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा-संस्थानों के छात्र-अध्यापक आदि थे, जो मौज-मस्ती करने, शराबनोशी करने और अपनी रातें गुलज़ार करने के लिए वहाँ आते थे।
अलिकसान्दर कुप्रीन ने अपने इस उपन्यास के शुरू में ही पाठकों को इसे समर्पित करते हुए लिखा है — मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को मेरी यह कहानी अनैतिक और अशोभनीय लगेगी, लेकिन फिर भी अपने दिल की गहराइयों से मैं इसे माताओं और युवाओं को समर्पित करता हूँ।
‘यामा’ यानी ‘गड्ढा’ नामक इस उपन्यास के नायक प्लातोनफ़ उपन्यास में ही एक जगह पर कहता है — इस कायनात में आदमी उच्चकोटि के श्रेष्ठ आनन्द को प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ है। इस दुनिया में आदमी ही भगवान है। दुनिया में आदमी अबाधित रूप से व्यापक प्रेम पाने के लिए स्वतन्त्र है। दुनिया का ज़र्रा-ज़र्रा उसके लिए ही बना है, चाहे वो पेड़ हो या आसमान, कुत्ता हो या कोई दूसरा आदमज़ात, यह सुन्दर प्यारी धरती, रोज़-रोज़ घटने वाले अपने अनूठे और विलक्षण चमत्कारों के साथ, अपने अनोखे और अजीब ओ ग़रीब जादू के साथ मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनी है।
कुप्रीन के ये शब्द उनके इस भरोसे और विश्वास को व्यक्त करते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का जन्म सिर्फ़ इसलिए होता है ताकि वह पूरी आज़ादी के साथ भले काम करके उच्चस्तरीय प्रेम, ख़ुशी और आनन्द को प्राप्त कर सके। उपन्यास का नायक प्लातोनफ़ आगे कहता है — लेकिन मनुष्य ने नीचता दिखाई और ख़ुद अपना तिरस्कार, अवमानना और अपमान किया और अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी को अन्धेरे और अभावों से भर दिया।
वेश्यावृत्ति को हमारी इस दुनिया का सबसे पुराना धन्धा या सबसे पुराना व्यवसाय कहा जाता है। पिछली दो सदियों में इस बारे में कई उपन्यास और शोधग्रन्थ लिखे गए हैं। सबसे पहले फ़्रांसीसी लेखक ओनेरो दे बालज़ाक ने वेश्यावृत्ति को लेकर बारह सौ पृठों का एक वृहदाकर उपन्यास लिखा था, जिसका नाम था — ‘वेश्याओं का वैभव और दैन्य’। 1837 से 1848 के बीच लिखे गए इस विशालकाय उपन्यास में बालज़ाक ने पेरिस की वेश्याओं के जीवन की सच्ची कहानियाँ लिखी थीं। हालाँकि बालज़ाक की यह रचना पूरी तरह से वेश्याओं पर केन्द्रित नहीं है। यह एक ऐसे ग़रीब युवक की कहानी है, जो अपना जीवन भीख माँगने से शुरू करता है और फिर पेरिस के अपराध जगत का शहंशाह बन जाता है। वह जुए के अड्डे चलाता है, वह कई वेश्यालयों का मालिक है, उसके बहुत से शराबख़ाने हैं और अपने इन काले कारनामों की वजह से उसे पेरिस के समाज में में बड़ा सम्मान और इज़्ज़त मिलती है और वह पेरिस के भद्र समाज का सबसे भद्र सदस्य बन जाता है। कहना चाहिए कि इस उपन्यास में एक आदमी के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ावों की बात की गई है और उसके भद्र रूप के पीछे छुपे उसके वास्तविक जीवन को वेश्यावृत्ति बताया गया है। यानी बालज़ाक ने अपने उपन्यास को पूरी तरह से वेश्याओं के जीवन पर केन्द्रित नहीं किया था।
वेश्याओं के जीवन को लेकर एक कहानी लिखने का विचार कुप्रीन के मन में 1888 में तब पैदा हुआ, जब उन्होंने पहले रूस के ओदेस्सा शहर की यात्रा की और बाद में वे 1990 में दो बरस के लिए रूस के कीव शहर में रहने के लिए पहुँचे। हालाँकि इससे पहले कुप्रीन रूस के ही साँक्त पितिरबूर्ग शहर में वेश्याओं के जीवन और उनकी बदहाली को देख चुके थे। लेकिन निकट से उनकी ज़िन्दगी को जानने और उनकी दुर्दशा, ज़िल्लत और फटेहाली-बदहाली को जानने-पहचानने का मौक़ा कुप्रीन को कीव में ही मिला।
कुप्रीन के मन में इस उपन्यास की कहानी धीरे-धीरे पकती रही। 1907 में उन्होंने यह उपन्यास लिखना शुरू किया। इन बीते बीस सालों में कुप्रीन ने ज़ारकालीन रूस में वेश्याजीवन का भली-भाँति अध्ययन कर लिया था। उन्हें मालूम था कि रूसी समाज में वेश्याओं को ‘समाज का कोढ़’ माना जाता है और सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए औरतों को लायसेंस जारी करने के बावजूद पुलिसकर्मी इस व्यवसाय में लिप्त औरतों का बुरी तरह से शोषण करते हैं। तो 1908 के शुरू में ही उनके इस उपन्यास के पहले भाग का पहला हिस्सा ‘तीन तिलंगों’ के नाम से ‘लिंग का सवाल’ नामक पत्रिका के जनवरी अंक में छपा। इस कथा के छपते ही तत्कालीन रूस के साहित्य संसार में हंगामा उठ खड़ा हुआ। कुप्रीन को पाठकों और अन्य लेखकों के ऐसे पत्र भारी संख्या में मिलने लगे, जिनमें उनकी लानत-मलामत की जा रही थी और समाज की गन्दगी उछालने के लिए पाठक उनपर अपना कहर बरपा रहे थे। लेकिन इस तरह के पत्रों के बावजूद कुप्रीन हताश नहीं हुए और कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने अपने उपन्यास के पहले भाग का दूसरा हिस्सा ‘जाग ज़माना’ नामक पत्रिका के अक्तूबर अंक में छपने के लिए भेज दिया। यह दूसरा हिस्सा छपने के बाद रूसी समाज में वेश्यावृत्ति को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पूरे रूस में इस सवाल पर खुलेआम विचार-विमर्श किया जाने लगा। आख़िरकार 1910 के शुरू में स्त्रियों की ख़रीद और बिक्री के सवाल पर एक अख़िल रूसी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के बाद कोठों में रहनेवाली औरतों की स्थिति और उनके व्यवसाय के सिलसिले में सरकार ने कुछ नए क़ानून बनाए और इन क़ानूनों के पालन पर कठोरता से निगाह रखी जाने लगी।
उपन्यास के दो हिस्से छपने के बाद रूसी पाठकों द्वारा की गई लानत-मलामत और छीछालेदर से अलिकसान्दर कुप्रीन बेहद व्यथित थे। लेकिन 1910 के शुरू में उन्होंने इस उपन्यास का दूसरा भाग लिखना शुरू कर दिया। उपन्यास का काम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। रूसी कवि कंसतांतिन बात्युशकफ़ के नाम लिखे एक पत्र में कुप्रीन ने यह स्वीकार किया है कि वे इस उपन्यास को आगे लिखना नहीं चाहते और जब भी वे उसे लिखने के लिए बैठते हैं तो वे अनमने हो जाते हैं और एक-दो पन्नों से ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं।
जब लम्बे समय तक ‘गड्ढा’ उपन्यास का दूसरा भाग सामने नहीं आया तो अन्य रूसी लेखकों ने कुप्रीन का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। रूसी अख़बारों में कुप्रीन से जुड़े कार्टून छपने लगे। यहाँ तक कि इप्पअलीन रपगोफ़ नामक एक लेखक ने 1913 में कुप्रीन के नाम से एक नक़ली उपन्यास लिखकर छपवा दिया, जिसका नाम था — गडढे का अन्त। इप्पअलीन रपगोफ़ की इस हरकत के बाद कुप्रीन ने उपन्यास का दूसरा भाग बड़ी तेज़ी से लिखा और 1914 में छपने के लिए प्रकाशक को दे दिया। लेकिन प्रकाशकों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। इन मजबूरियों के चलते ही क़रीब साल भर बाद ‘गड्ढा’ उपन्यास का दूसरा भाग छपकर सामने आया।
फिर 1917 में बारह खण्डों में कुप्रीन की रचनावली छपी। इस रचनावली के बारहवें खण्ड में ‘यामा’ यानी ‘गड्ढा’ नामक उपन्यास अपने पूरे स्वरूप में छपकर सामने आया था। पूरा उपन्यास छपने के बाद पत्र-पत्रिकाओं में उसकी समीक्षाएँ भी सामने आने लगीं। कुप्रीन के इस उपन्यास की तुलना फ़्रांसीसी लेखक गी दे मोपांसा के 1881 में प्रकाशित उपन्यास ‘टेलर के चकले’ और मकसीम गोरिकी की 1999 में प्रकाशित कहानी ‘वासका क्रासनी’ से की जाने लगी। लेखक ल्येफ़ तलस्तोय ने कहा — मुझे कुप्रीन के उपन्यास में एक अलग ही रस मिल रहा है। कुप्रीन की भाषा शैली ऐसी है कि उनकी किसी भी रचना को मैं अन्त तक पूरी पढ़कर ही उठता हूँ। रूसी लेखक करनेय चुकोव्स्की ने लिखा :
“कुप्रीन ने हमारे समकालीन समाज के मुँह पर एक बड़ा तमाचा मारा है। यह ठीक है कि ‘वेश्याएँ घृणित होती हैं’, लेकिन जितनी ज़्यादा वे घृणित हैं, हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा शर्म की बात है। उन्हें बचाने या उनका पुनरुद्धार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका पुनरुत्थान करने की जगह हमें उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की बात सोचनी चाहिए। अपने सामाजिक जीवन को हमें इस तरह से बदलने की ज़रूरत है कि उसमें आगे कोई भी छेद बाक़ी न रह जाए।”
फ़्रांसीसी लेखक रोम्याँ रोलां ने ‘यामा’ यानी ‘गड्ढा’ पढ़ने के बाद कुप्रीन को लिखा :
“मैं आपकी साहित्यिक प्रतिभा से अभिभूत हूँ और आपकी गहरी मानवीय समझ की प्रशंसा करता हूँ। आपकी भाषा-शैली एक ऐसा दुर्लभ और विशिष्ट उपहार है, जो आपके पूरे समाज को किताबों के पन्नों पर जीवन्त उतार देता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो हमारे ज़माने की महानताओं से भी ऊपर उठकर उनके पार सुदूर भविष्य के भीतर झाँक सकते हैं। मैंने जब आपके इस ‘गड्ढे’ को पूरे यूरोप के सिलसिले में देखा तो मुझे लगा कि हमारा पूरा यूरोप ही एक विशाल वेश्यालय में बदल चुका है, जो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा।”
1915 में ख़ुद अलिकसान्दर कुप्रीन ने अपने इस उपन्यास का मूल्यांकन करते हुए कहा था :
“मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है। वेश्यावृत्ति किसी युद्ध या महामारी से भी अधिक भयानक बात है। ल्येफ़ तलस्तोय ने मेरा यह उपन्यास पढ़ने के बाद मुझसे कहा — “यह गन्दगी है।” हाँ, यह गन्दगी है, लेकिन इस गन्दगी को हमें ख़ुद ही साफ़ करना होगा। अगर ल्येफ़ तलस्तोय जैसा बड़ा लेखक इस गन्दगी के बारे में लिखता, तो सचमुच एक ज़रूरी और महत्त्वपूर्ण काम होता। खेद है कि मेरी क़लम कमज़ोर है। मैं तो केवल वेश्याओं की ज़िन्दगी के कुछ पन्नों को खोलकर उन्हें पढ़वाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, अब उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है, जैसाकि अब तक होता रहा है। आख़िर वेश्याएँ भी मनुष्य हैं …”
अन्त में मैं पाठकों को इतना और बताना चाहता हूँ कि इस उपन्यास पर अब तक तीन फ़िल्में बन चुकी हैं और एक टेलीविजन सीरीयल भी बनाया जा चुका है। दुनिया भर के नाट्य मंचों पर अकसर इस उपन्यास पर आधारित नाटकों के प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन हमारे भारत के किसी नाट्य-निर्देशक ने इस रचना पर नाटक खेलने की हिम्मत अभी तक नहीं दिखाई है। दुनिया की चालीस से ज़्यादा भाषाओं में इस उपन्यास का अनुवाद हो चुका है। भारत में, पिछले नब्बे सालों में हिन्दी में इसके अब तक सिर्फ़ चार ही संस्करण छपे हैं और यह उपन्यास बार-बार पाठकों के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। मेरे बार-बार अनुरोध करने पर अनुज्ञा बुक्स ने इसे छापने का बीड़ा उठाया है और मुझे लगता है कि यह उपन्यास हिन्दी में अब पाठकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। सादर।
मई, 2024
अनिल जनविजय
Additional information
Additional information
| Product Options / Binding Type |
|---|
Related Products
-
-8%
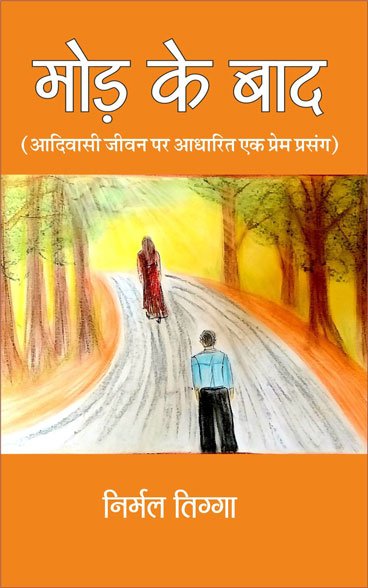 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewFiction / कपोल -कल्पित, Jharkhand / झारखण्ड, Novel / उपन्यास, Paperback / पेपरबैक, Tribal Literature / आदिवासी साहित्य
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewFiction / कपोल -कल्पित, Jharkhand / झारखण्ड, Novel / उपन्यास, Paperback / पेपरबैक, Tribal Literature / आदिवासी साहित्यMODE KE BAAD / मोड़ के बाद – आदिवासी हिंदी उपन्यास
₹299.00Original price was: ₹299.00.₹275.00Current price is: ₹275.00. -
-8%

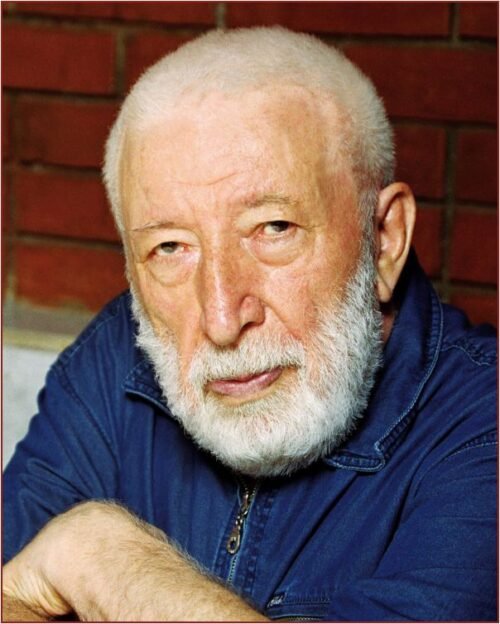 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewClassics / क्लासिक्स, Fiction / कपोल -कल्पित, New Releases / नवीनतम, Novel / उपन्यास, Paperback / पेपरबैक, Russian Classics / Raduga / Pragati / उत्कृष्ट रूसी साहित्य, Top Selling, Translation (from English or Foreign) / अंग्रेजी अथवा अन्य विदेशी भाषाओं से अनुदित
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewClassics / क्लासिक्स, Fiction / कपोल -कल्पित, New Releases / नवीनतम, Novel / उपन्यास, Paperback / पेपरबैक, Russian Classics / Raduga / Pragati / उत्कृष्ट रूसी साहित्य, Top Selling, Translation (from English or Foreign) / अंग्रेजी अथवा अन्य विदेशी भाषाओं से अनुदितMera Daghestan (Both Vols.) / मेरा दग़िस्तान (दोनों खण्ड)
₹599.00Original price was: ₹599.00.₹550.00Current price is: ₹550.00. -
-20%

 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Bhojpuri / भोजपुरी, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, New Releases / नवीनतम, Novel / उपन्यास, Panchayat / Village Milieu / Gramin / पंचायत / ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, Paperback / पेपरबैक, Stories / Kahani / कहानी
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Bhojpuri / भोजपुरी, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, New Releases / नवीनतम, Novel / उपन्यास, Panchayat / Village Milieu / Gramin / पंचायत / ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, Paperback / पेपरबैक, Stories / Kahani / कहानीJugesar
₹144.00 – ₹216.00
जुगेसर -
Sale

 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick View
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick View
