





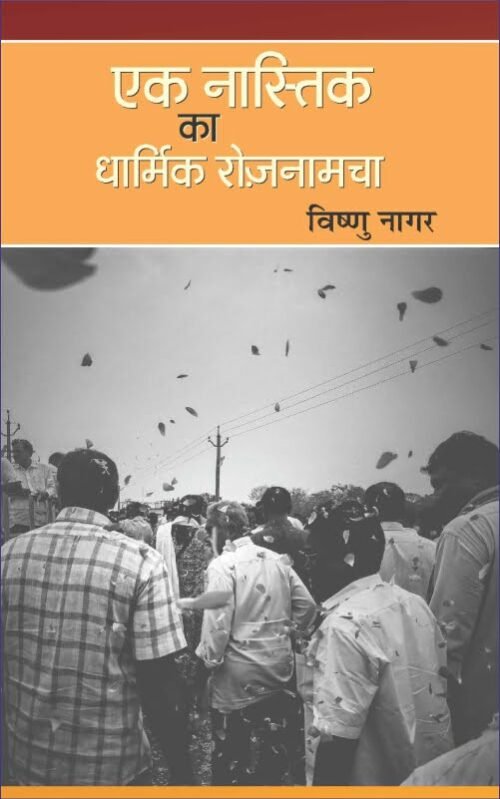

Ek Nastik ka Dharmik Rojnamcha / एक नास्तिक का धार्मिक रोजनामचा
₹245.00 – ₹425.00
FREE SHIPMENT FOR ORDER ABOVE Rs.149/- FREE BY REGD. BOOK POST
Read eBook in Mobile APP
नेमाड़े के बहाने हिंदू धर्म
अदिनांकित
उदयन वाजपेयी द्वारा संपादित तथा रजा फाउण्डेशन के कार्यकारी न्यासी अशोक वाजपेयी द्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘समास’ का दसवाँ अंक आया है जिसमें मराठी लेखक-विचारक भालचन्द्र नेमाड़े की 34 पृष्ठ लम्बी बातचीत छपी है। इसे पूरा पढ़े बिना रह न सका। 76 वर्षीय नेमाड़े की बातचीत का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है– भारतीय साहित्य परंपरा में काव्य का प्राधान्य, गद्य-परंपरा, भारतीय साहित्य परंपरा में उपन्यास, कई रामायणों का होना, ईश्वर तथा भक्त का संबंध, देसीपन की संकल्पना तथा उनके ताजा उपन्यास ‘हिंदू : जगण्याची समृद्ध अडगल’ के पहले भाग पर चर्चा, जिसके अन्य भागों पर लेखक अभी काम कर रहा है। हिंदू धर्म, जाति-व्यवस्था का समर्थक है, जिसका जहर भारत के अन्य धर्मों में भी फैला है। वह कहते हैं – ‘अब जाति-भेद नष्ट हो जाने चाहिए, जातीयता एक विषैली प्रवृृत्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं’ लेकिन उनका यह कहना भी है कि जाति-व्यवस्था पहले लचीली थी और आज जाति-व्यवस्था को चाहकर भी उखाडऩा संभव नहीं है। वे इसे ‘असंभव’ मानते हैं। ‘असंभव चीजें आप कैसे करेंगे? महावीर, बुद्ध, नाथ, वारकरी, कबीर, महानुभाव फु ले, अम्बेडकर में से कोई भी इन जातियों को समूल तो छोडिय़े, उनकी ऊपरी सतह तक भी नष्ट नहीं कर पाया है। उल्टे फूले, अम्बेडकर के बाद जातियाँ और मजबूत हुई हैं। ये मराठी प्रगतिशीलों को बताने की जरूरत नहीं। हमारे उपखंड में रहने वाली सारी जनता– ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू इन सबका जाति-व्यवस्था का एक ढाँचा है, आदि-आदि।
नेमाड़े कोई हिंदू उग्रवादी-जातिवादी नहीं हैं मगर उनके कई विचार विवादास्पद हैंं। जैसे वह यह कहते हैं कि पिछले पाँच हजार वर्षों में भारत में अनेक बड़े जनसमूह आते रहे, बसते रहे। इनमें से सब भाषा, धर्म, देवी-देवता, रीति-रिवाज, खाने-पीने, पहनने-ओढऩे, सजने-सँवरने के हजारों तरीके लाते रहे और जाति-व्यवस्था ने इन सबकी स्वायत्तता को सुरक्षित रखा। वह मानते हैं इस जैसी कोई और व्यवस्था भारत के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। पहले केवल एक आधारभूत संरचना के रूप में जाति-व्यवस्था का पालन किया जाता था। इस व्यवस्था की जगह पूँजीवादी वर्ग-व्यवस्था इससे ज्यादा बुरी विषैली सिद्ध होगी। उनके अनुसार अस्पृश्यता, जाति-व्यवस्था की देन नहीं है, हालाँकि यह पिछले लगभग हजार वर्षों से चली आ रही है। इसके ऐतिहासिक कारण हैं लेकिन उन कारणों में नेमाड़े नहीं जाते।
श्री नेमाड़े चूँकि हिंदूत्ववादी विचारहीन व्यक्ति नहीं हैं, पढ़े-लिखे, उदार, विचारों के धनी हैं, विद्वान हैं तो संभव है, वह सही हों। हो सकता है कि पहले जाति-व्यवस्था लचीली रही हो, समावेशी रही हो लेकिन अगर श्री नेमाड़े के मुताबिक ही यह व्यवस्था पिछले हजार वर्षों से लचीली रही है, फिर भी अस्पृश्यता को प्रोत्साहित-संरक्षण देती रही है, मुझ तक तो उसका यही रूप पहुँचा है। यह सही हो सकता है कि इस ढाँचे को तोडऩा आसान नहीं है, न अभी यह टूटा है, न फिलहाल इसके टूटने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल किसी व्यवस्था का टूटना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसे तोडऩे वाले साहसी, विचारवान, प्रभावी व्यक्ति थे, संत थे। वे एक ‘उत्प्रेरक’ का काम कर सकते हैं लेकिन बाकी काम तो राजनीतिक-सामाजिक ढाँचे के अंदर ही होता है। आज हमारा समाज किस हद तक लोकतान्त्रिक है, गतिमान है, राजनीतिक रूप से जागरूक है, अधिकारों के प्रति सचेत है, तकनालाजी से प्रभावित-प्रेरित है मगर पूँजीवाद-उपभोक्तावाद की जकड़ में है। आज समाज की गतिहीनता को तोडऩे के लिए जितनी शक्तियाँ तरह-तरह से लगी हुई हैं, पहले कभी सक्रिय नहीं थीं। पूँजीवाद ने इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन भी नहीं किया था और लोगों का आवागमन भी सुगम नहीं बनाया था। विज्ञान-तकनालाजी का वर्चस्व इतना पहले कभी नहीं था, जितना आज है। राजनीतिक ताकतें कभी इतनी गतिशील नहीं थीं, जितनी आज हैं। उपभोक्तावाद का प्रभाव इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ा था, जितना आज है। संचार-साधनों की पहुँच इससे पहले कभी इतनी नहीं थी, जितनी आज है। और छोटी-से-छोटी जगहों पर रहने वाले स्त्री-पुरुषों, लड़के-लड़कियों में अभाव का वैसा तीव्र बोध नहीं था, जैसा कि आज है।
अत: आज कई शक्तियाँ एक-दूसरे के विरोध और सहभाग में खड़ी हैं। पहले पिछड़े तथा दलित कभी इतने संगठित नहीं थे, जितने आज हैं। कहीं यह अनुपात ज्यादा है, कहीं कम। पिछड़े तो पूरे हिंदी भाषी राज्यों में संगठित हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह दलित कहीं और संगठित नहीं हैं। इसी बीच मजदूरों-कर्मचारियों के वर्ग आधारित संगठन बहुत हद तक कमजोर और नष्ट हुए हैं। बुनियादी परिवर्तन के आंदोलन कमजोर हुए हैं। उधर हिन्दू कट्टरवाद के साथ अन्य किस्म का कट्टरवाद भी बढ़ा है। जो जातियाँ समृद्ध हुई हैं, उन्होंने अपने से ऊपर के वर्गों की पिछड़ी सामाजिक दृष्टि को अपना लिया है, क्योंकि वे मानती हैं कि वर्चस्ववादी वर्गों के तौर-तरीकों से ही वे भी अपने को मजबूत कर सकती हैं। जाति-पंचायतों-खाप पंचायतों ने अपने कट्टर कानून लादने शुरू किए हैं तो तमाम तरह के द्वंद्वों-अंतद्र्वंद्वों में फँसी नयी पीढ़ी व्यक्तिगत तरीके से ही सही, इसका विरोध कर रही है, जिसे बाहरी समर्थन मिल रहा है। विस्थापित जन शहरों में आ रहे हैं और उनमें जाति-भाषा-धर्म की हदों को तोडऩे का स्वाभाविक भाव पैदा हो रहा है। ट्रेनों के जनरल डिब्बों में लोग जानवरों की तरह ठुँसे रहते हैं, उनका जाति-धर्म एक झटके में थोड़े समय के लिए ही सही मगर टूट जाता है। धर्म तथा जाति की दीवारें तोड़कर नये लोग साथ काम कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। विवाह टूट भी रहे हैं, अवैध कहे जाने वाले संबंध भी बन रहे हैं। पिछले सौ-डेढ़ सौ सालों में प्रवासी भारतीयों की अपनी मजबूरियों के कारण जाति-धर्म देश के बन्धन टूटे थे, अब बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया देश के अंदर भी चल रही है। यह एक लम्बी-तकलीफदेह और किसी हद तक हिंसक प्रक्रिया है, इसमें कई बाधाएँ हैं मगर जो काम महावीर-बुद्ध-कबीर आदि-आदि नहीं कर पाए, वह शायद यह सुदीर्घ, परस्पर विरोधी तेज गति वाली प्रक्रिया कर सके। जो हो नहीं सका पहले, वह होगा नहीं कभी, यह मानना गलत है। हाँ, लेकिन जो जातियों के टूटने से बनेगा, बनने की कोशिश में होगा, वह सुखद ही होगा, यह कहना कठिन है लेकिन टूटना, न बनने से ज्यादा तकलीफदेह तो होता ही है।
- Description
- Additional information
Description
Description
…विष्णु नागर…
जन्म : 14 जून, 1950। बचपन और छात्र जीवन शाजापुर (मध्यप्रदेश) में बीता। 1971 से दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकारिता। नवभारत टाइम्स तथा हिंदुस्तान, कादंबिनी, नईदुनिया, ‘शुक्रवार’ समाचार साप्ताहिक से जुड़े रहे। भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य एवं महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य। इस समय स्वतंत्र लेखन। प्रकाशित कृतियाँ : कविता संग्रह – मैं फिर कहता हूँ चिड़िया, तालाब में डूबी छह लड़कियाँ, संसार बदल जाएगा, बच्चे, पिता और माँ, कुछ चीज़ें कभी खोई नहीं, हँसने की तरह रोना, घर के बाहर घर, जीवन भी कविता हो सकता है तथा ‘कवि ने कहा’ श्रृंखला में कविताओं का चयन। कहानी संग्रह – आज का दिन, आदमी की मुश्किल, कुछ दूर, ईश्वर की कहानियाँ, आख्यान, रात-दिन, बच्चा और गेंद, पापा मैं ग़रीब बनूँगा। व्यंग्य संग्रह – जीव-जंतु पुराण, घोड़ा और घास, राष्ट्रीय नाक, देशसेवा सेवा का धंधा, नई जनता आ चुकी है, भारत एक बाज़ार है, ईश्वर भी परेशान है, छोटा सा ब्रेक तथा सदी का सबस बड़ा ड्रामेबाज। उपन्यास – आदमी स्वर्ग में। आलोचना – कविता के साथ-साथ। जीवनी – असहमति में उठा एक हाथ (रघुवीर सहाय की जीवनी)। लेख और निबंध संग्रह – हमें देखतीं आँखें, आज और अभी, यथार्थ की माया, आदमी और उसका समाज, अपने समय के सवाल,ग़रीब की भाषा, यथार्थ के सामने। साक्षात्कारों की पुस्तक –‘मेरे साक्षात्कारः विष्णु नागर’। ‘सहमत’ संस्था के लिए तीन संकलनों तथा रघुवीर सहाय पर पुस्तक का संपादन। परसाई की चुनी हुई रचनाओं का संपादन। सुदीप बनर्जी की कविताओं के चयन का संपादन लीलाधर मंडलोई के साथ। मृणाल पांडे के साथ ‘कादंबिनी’ मे प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण लेखकों द्वारा चयनित विश्व की श्रेष्ठ कहानियों का संचयन – ‘बोलता लिहाफ’। इसके अलावा नवसाक्षरों के लिए अनेक पुस्तकों का संपादन एवं लेखन। हाल ही में किशोरों के लिए भी कुछ पुस्तिकाएँ लिखी हैं। मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, शमशेर सम्मान, व्यंग्य श्री सम्मान, दिल्ली हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान, शिवकुमार मिश्र स्मृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पत्रकारिता शिरोमणि, रामनाथ गोयनका सम्मान पत्रकारिता के लिए समेत कई सम्मान। सम्पर्क : ए-34, नवभारत टाइम्स अपार्टमेंट, मयूर विहार फ़ेज़-1, नई दिल्ली-110091।
Additional information
Additional information
| Product Options / Binding Type |
|---|
Related Products
-
-38%

 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewCriticism Aalochana / आलोचना, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, Top Selling
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewCriticism Aalochana / आलोचना, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, Top SellingSamkaleen Vimarshvadi Upanyas / समकालीन विमर्शवादी उपन्यास
₹600.00Original price was: ₹600.00.₹375.00Current price is: ₹375.00. -
-20%

 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Biography / Jiwani / जीवनी, Criticism Aalochana / आलोचना, Hard Bound / सजिल्द, Paperback / पेपरबैक, Renaissance / Navjagran / Rashtravad / नवजागरण / राष्ट्रवाद
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Biography / Jiwani / जीवनी, Criticism Aalochana / आलोचना, Hard Bound / सजिल्द, Paperback / पेपरबैक, Renaissance / Navjagran / Rashtravad / नवजागरण / राष्ट्रवादRashtriyata sai Antarrashtriyata
₹400.00 – ₹700.00
राष्ट्रीयता से अन्तर्राष्ट्रीयता -
-40%

 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewHard Bound / सजिल्द, Stories / Kahani / कहानी, Translation (from Indian Languages) / भारतीय भाषाओं से अनुदित
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewHard Bound / सजिल्द, Stories / Kahani / कहानी, Translation (from Indian Languages) / भारतीय भाषाओं से अनुदितSurinder Rampuri : Chuninda Kahanian
सुरिंदर रामपुरी : चुनिन्दा कहानियाँ (मूल पंजाबी से डॉ. सुभाष नीरव द्वारा अनूदित)₹480.00Original price was: ₹480.00.₹290.00Current price is: ₹290.00. -
Art and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Criticism Aalochana / आलोचना, Hard Bound / सजिल्द, New Releases / नवीनतम, Tribal Literature / आदिवासी साहित्य
Rashtra Purush Somji Bhai Damor – Jeewni avam anya Aalekh राष्ट्रपुरुष सोमजीभाई डामोर – जीवनी एवं अन्य आलेख – Hindi Biography
₹600.00Original price was: ₹600.00.₹415.00Current price is: ₹415.00.


